Table of Contents
परिचय-
सरसों का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विशेष स्थान है। देश की तेल वाली फसलों के कुल उत्पादन में सरसों का योगदान 27 प्रतिशत है। सरसों रबी मौसम में उगाए जाने वाली मुख्य फसल है। इसकी खेती सिंचित एवं संरक्षित नमी वाले बारानी क्षेत्रों में की जाती है। कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों के लगातार प्रयासों से सरसों के उत्पादन में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। यह फसल कम लागत और कम सिंचाई की सुविधा में भी अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ देती है। इसको अकेले या सहफसली खेती के रूप में भी बोया जा सकता है। इसकी खेती सीमित सिंचाई की दशा में अधिक लाभदायक होती है।
भूमि एवं जलवायु –
समतल और अच्छे जल निकास वाली बलुई और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। जमीन गहरी और इसमें जलधारण की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। भारत में सरसों की खेती शरद ऋतु में की जाती है। इसको 18-25 डिग्री. सें.ग्रे. तापमान की आवश्यकता होती है। यह आर्द्र एवं शुष्क दोनों ही क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। अधिक उत्पादन के लिए सरसों को ठण्डे तापमान, साफ, खुला आसमान तथा पर्याप्त मृदा आर्द्रता की आवश्यकता होती है।
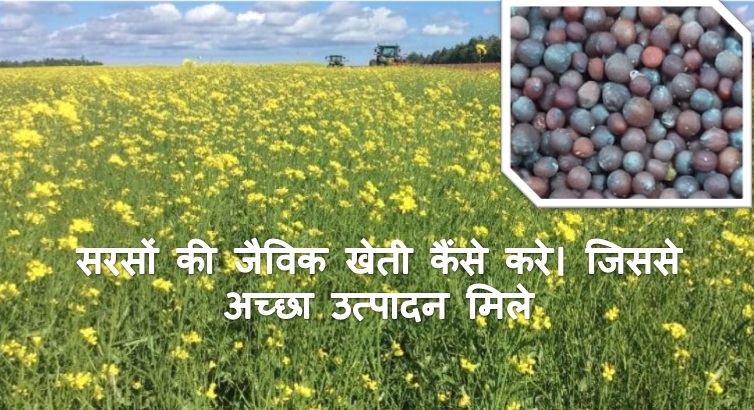
उन्नतशील किस्में –
कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा संस्तुत उन्नत किस्मों का चयन करें। जैसे – टी..59 (वरुणा), आर.एच..8812, पूसा विजय (एन.पी.जे. 93), पूसा मस्टर्ड 22, आर.एस..38, पूसा करिश्मा और पूसा महक आदि।
टी-59 (वरूणा) –
मध्यम कद वाली, शाखाऐं फैली हुई, पकने की अवधी 125-140 दिन, पत्तियाँ चौड़ी व छोटी, दाना काला, असिंचित दशा में 10-15 कुन्टल तथा सिंचित दशा में 15-18 कुन्टल प्रति हेक्टेयर औसत उपज, तेल की मात्रा 36 प्रतिशत तथा सफेद रोली रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली किस्म है।
आर.एच.-30 –
यह किस्म सिंचित व असिंचित दोनों दशा में गेंहूं, जौ, चना सह-फसली खेती तथा देर से बुवाई के लिए उपर्युक्त होती है। पौधे 196 सें.मी. ऊँचे, 5-7 प्राथमिक शाखाआ वाली, पत्तियाँ मध्यम आकार तथ्130-135 दिन में पकने वाली मोटे दाने वाली तथा 15-20 अक्टूबर तक बुवाई हेतु उपयुक्त होती है।
पी.आर.-15 (क्रान्ति) –
सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में बुवाई हेतु उपयुक्त, पौधे 155-200 सें.मी. ऊँचे, पत्तियां रोयेदार, तना चिकना और फूल हल्के रंग के होते है। सिंचित क्षेत्रों में 15-18 कुन्टल उपज प्राप्त होती है। दाना मोटा कत्थई एवं तेल की मात्रा 40 प्रतिशत, 125-135 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। आल्टरनेरिया ब्लाईट एवं आरा मक्खी अवरोधी। वरूणा किस्म की अपेक्षा पाले के प्रति सहनशील एवं तुलासिता व सफेद रोली रोधक होती है।
बायो-902 –
यह किस्म 160-180 सें.मी. ऊँची, सफेद रोली, मुरझान व तुलासिता रोगों को प्रकोप अन्य किस्मों की अपेक्षा कम, फलियाँ पकने पर दानों का नहीं झड़ना, दाना काला व भूरा होता है। उपज 18-20 कुन्टल प्रति हेक्टेयर, पकने का समय 130-140 दिन एवं तेल 38-40 प्रतिशत, तेल खाने में उपयुक्त, फलियों में 12-15 दाने होते है।
लक्ष्मी –
यह किस्म 145 दिनां में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पत्तियां छोटी पतली व ऊपर की तरफ उठी होती हैं। इस किस्म की फलियाँ एवं बीज का दाना मोटा तथा कले रंग का होता है। यह सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहती है। इस किस्म से 18-20 कुन्टल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त की जा कसती है।
पूसा अग्रणी –
यह एक जल्दी पकने वाली किस्म है। इसका दाना मोटा व भूरे रंग का होता है, फूल छोटे एवं चमकीले पीले होते है। इस किस्म की बुवाई सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है तथा 15-18 कुन्टल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज ली जा सकती है।
खेत की तैयारी : बारानी खेती के लिए पिहली जुताई वर्षा ऋतु में मिट्टी पलटने वाले हल से करें। समय-समय पर खेत की स्थिति के अनुसार 3-4 जुताई करें। सिंचित खेतों के लिए खेत की तैयारी बुवाई के 3-4 सप्ताह पहले आरम्भ करें।
खेत की तैयारी –
सरसों को भुरभुरी मृदा की आवश्यकता होती है। अतः खरीफ की कटाई के बाद एक गहरी जुताई करके 2-3 जुताई हल या हेरों से करें। जुताई के बाद पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें ताकि बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी मौजूद रहे और बीज का सही जमाव हो सके।
भूमि उपचार –
दीमक, सफेद गिडार आदि कीटों की रोकथाम के लिए बुआई पूर्व नीम की खली 7-8 कि्ंव. प्रति हेक्टे. की दर से प्रयोग करें। फफूंद रोगों से बचाव हेतु 3-5 कि.ग्रा. ट्राईकोर्डमा को 200-250 कि.ग्रा. गोबर की खाद में मिलाकर खेत में मिला दें।
बुआई का समय –
भूमि, जलवायु, सिंचाई के साधनों तथा प्रजातियों के अनुसार सरसों की बुआई अलग-अलग समय पर की जाती है। बुआई के लिए उपयुक्त तापमान 25-26 डिग्री. सें.ग्रे. है। अतः सरसों की बुआई सामान्यतः सितंबर के अंतिम सप्ताह से 20-25 अक्टूबर तक कर लेनी चाहिए।
बीज की मात्रा –
सिंचित क्षेत्रों में 4-5 कि.ग्रा. एवं असिंचित क्षेत्रों में 5-6 कि.ग्रा. बीज प्रति हेक्टे. प्रयोग करना चाहिए।
बीज का उपचार –
बीजजनित रोग से बचाव के लिए बीजामृत या ट्राइकोडर्मा 8-10 ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से बीजशोधन करें। वातावरण की नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु सरसों के बीजों को एजोस्पाइरिलम तथा फॉस्फोरस जीवाणु कल्चर से उपचारित करना चाहिए। गलन रोग से बचाव हेतु लहसुन के दो प्रतिशत सत (20 ग्राम लहसुन सत को एक लीटर) से बीजों का उपचार करें।
बुआई विधि –
सरसों की बुआई देशी हल या सीडड्रिल द्वारा कतारों में करनी चाहिए । कतार से कतार की दूरी 30.45 सेमी. तथा पौधे से पौधे की दूरी 15.20 सेमी. रखनी चाहिए। सिंचित क्षेत्र में बीज की गहराई 4.5 सेंमी. तथा असिंचित क्षेत्र में 2.3 सेमी. नमी के अनुसार रखनी चाहिए। बीज ढ़कने के लिए हल्का पाटा लगा देना चाहिए।
खाद एवं जैविक उर्वरक –
सिंचित क्षेत्रों में 80-100 कि्ंव. ट्राइकोडर्मा द्वारा उपचारित सड़ी गोबर की खाद अथवा 50-60 क्विं. कम्पोस्ट प्रति हेक्टे. खाद को बुआई से 15 दिन पूर्व खेत में जुताई करके मिला देना चाहिए। 3-5 कि.ग्रा. अजैटोबैक्टर/एजोस्पोरिलम जैविक उर्वरक का प्रयोग जैविक खाद में मिलाकर भूमि में जुताई के समय करना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए सीमित मात्रा में प्राकृतिक जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। पहली व दूसरी सिंचाई के साथ जीवामृत तथा वेस्ट डिकम्पोजर 500 लीटर घोल का प्रयोग करें।
निराई-गुडाई एवं छँटाई –
बुआई के 20-25 दिन के अन्दर घने पौधों को निकालकर उनकी आपसी दूरी 15 सेमी. होनी चाहिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए एक निराई.गुड़ाई पहली सिंचाई के बाद करें।
सिंचाई –
पहली सिंचाई खेत की नमी, प्रजाति और मृदा के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए 30-40 दिन के बीच फूल बनने के समय एवं दूसरी सिंचाई 60-70 दिन के बीच फली बनने पर करनी चिहए।
कीट एवं रोग प्रबंधन –
सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट निम्न प्रकार हैं.
आरा मक्खी कीट –
काले रंग के ग्रब गोलाकार छेद करके पत्तियों को क्षति पहुँचाते हैं।
इनकी रोकथाम हेतु गौमूत्र, गोबर, वनस्पति (ऑक, धतूरा, नीम पत्ती आदि) से तैयार किया गया तरल कीटनाशी 10 प्रतिशत घोल का 10-15 दिन के अन्तर पर छिडक़ाव करें।
नीम ऑयल 3.5 मिली. प्रति लीटर घोल का दो बार छिड़काव करें। हानिकारक कीटों की रोकथाम हेतु लाभदायक.परभक्षी कीटों का संरक्षण करें।
माहू कीट-
फूल आने की अवस्था में अनुकूल मौसम होने पर इसका प्रकोप पत्तियों के निचली सतह तथा पुष्प.चक्र पर होता है। यह पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों का रस चूसता है तथा एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ देता है जिससे पौधा कमजोर हो जाता है तथा उस पर फलियाँ व दाने नहीं बन पाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सरसों की अगेती बुआई 25 अक्टूवर तक अवश्य कर लें। पौधों में उचित फासला रखें।
नीम की पत्ती/निमोली सत/वनस्पति कीटनाशक 10 प्रतिशत घोल का 1.2 छिड़काव फूल आने से पहले करें।
अधिक प्रकोप की संभावना में मैटाराईजियम जैव कीटनाशक का 3.4 कि.ग्रा. प्रति हेक्टे. की दर से छिडकाव करें।
बालदार (गिडार) उपचार –
यह कीट पत्तियों पर गुच्छों में अण्डे देता है। इसमें से निकलने वाली सुण्डी के शरीर पर नुकीले बाल निकलते हैं। यह सुण्डी झुण्ड में पत्तियों को खाती है तथा नुकसान पहुँचाती हैं।
इसकी रोकथाम के लिए –
- प्रारम्भिक अवस्था में अण्डे एवं छोटी सुण्डी सहित पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए।
- छोटी अवस्था में सुण्डी पर अग्निअस्त्र का छिड़काव करें।
- बिवेरिया बेसियाना 3.4 कि.ग्रा. प्रति हेक्टे. छिडक़ाव करें।
चित्रित कीट (पेंटेड बग) –
इस कीट का प्रकोप प्रारंभिक अवस्था से लेकर बढ़वार की अवस्था तक पाया जाता है। यह एक चित्तीदार बग है जो पत्तियों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुँचाती है। अधिक प्रकोप होने पर फूल और फली नहीं बन पातीं तथा पौधा सूख जाता है।
इसकी रोकथाम के लिए-
- इस कीट की रोकथाम हेतु नीम की पत्ती/निमोली सत का छिड़काव करें।
- नीम ऑयल या वनस्पति तरल कीटनाशी का 10-15 दिन के अन्तर पर छिडक़ाव करें।
